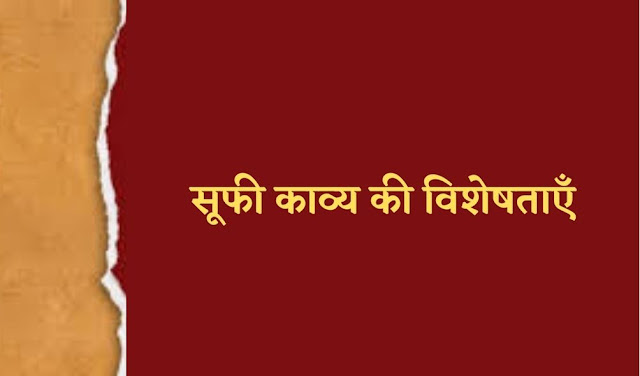 |
| सूफी काव्य की विशेषताएँ ,Sufi Kavya Ki Visheshtayein |
सूफी काव्य की विशेषताएँ | Sufi Kavya Ki Visheshtayein
सूफी काव्यधाराः
सूफी काव्य: सूफी काव्यधारा निर्गुण भक्ति की दूसरी शाखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे प्रेमाश्रयी शाखा के रूप में संज्ञापित किया है। संत कवियों ने जहाँ एक ओर सर्वसाधारण के लिए भक्ति के साधारण मार्ग की प्रतिष्ठा की, वहीं दूसरी ओर सूफी फकीरों ने हिन्दू-मुस्लिम एकता का प्रयास किया। इस कार्य में संत कवियों की अपेक्षा उन्हें आशातीत सफलता मिली। सूफी फकीर दोनों संस्कृतियों के सुंदर सामंजस्य के पक्षधर थे। इनके साहित्य की आत्मा विशुद्ध भारतीय है, यद्यपि इसमें प्रेम और धर्म की विदेशी साधना भी घुलमिल गई है।
सूफीमत इस्लाम धर्म की एक उदार शाखा है जिसका उदय इस्लाम के अस्तित्व में आने के बाद हुआ। सूफियों के चार सम्प्रदाय भारत में मिलते हैं- चिश्ती सम्प्रदाय, सोहरावर्दी सम्प्रदाय (12वीं शती), कादरी सम्प्रदाय (15वीं शती), नक्सबंदी सम्प्रदाय (15वीं शती)। इन सूफी संतों के उच्च विचार, सादा जीवन और व्यापक प्रेम के तत्वों ने भारतीय जन-जीवन को आकृष्ट किया। इन सूफियों ने ‘अनलहक’ अर्थात् ‘मैं ब्रह्म हूँ’ की घोषणा की। ठीक यही बात भारत के अद्वैतवादी भी कह रहे थे। अद्वैतवादियों ने घोषणा की- ‘अहम् ब्रह्मास्मि’ अर्थात् ‘मैं ब्रह्म हूँ’। इसलिए अपने दार्शनिक आधार के कारण सूफी संत भी भारतीय भक्ति आन्दोलन में परिगणित किए गए।
हिन्दी की निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा अर्थात् सूफी काव्यधारा ने भक्तिकालीन काव्य को प्रेम दर्शन की नवीन दृष्टि प्रदान की है। इन कवियों का ध्यान मानव जीवन के सर्वांग विकास पर था। सूफियों की मान्यता थी कि मनुष्य हृदय की क्षुद्रताओं को प्रेम ही हटा सकता है। ‘‘मानुष प्रेम’ का जीवन-दर्शन ही इन सूफियों का एकमात्र उद्देश्य था। इस धारा के सभी मुसलमान सूफी कवियों में धार्मिक संकीर्णता का नामों-निशान तक नहीं है। इनका समूचा साहित्य एक व्यापक विश्व बंधुत्व और विश्व दृष्टि की रचनात्मक अभिव्यक्ति है। इनकी दृष्टि में लौकिक प्रेम और ईश्वरीय प्रेम में कोई फर्क नहीं है। इसलिए यह कहना अनुचित होगा कि इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए सूफियों ने काव्य लिखे हैं।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि ‘‘सौ वर्ष पूर्व कबीरदास हिन्दू और मुसलमान दोनों के कट्टरपन को फटकार चुके थे। पंडित और मुल्लाओं की तो नहीं कह सकते पर साधारण जनता राम और रहीम की एकता मान चुकी थी। साधुओं और फकीरों को दोनों दीन के लोग आदर और मान की दृष्टि से देखते थे। साधू या फकीर भी सर्वप्रिय वे ही हो सकते थे जो भेदभाव से परे दिखाई पड़ते थे। बहुत दिनों तक साथ-साथ रहते-रहते हिन्दू और मुसलमान एक-दूसरे के सामने अपना-अपना हृदय खोलने लगे थे, जिससे मनुष्यता के सामान्य भावों के प्रवाह में मग्न होने और मग्न करने का समय आ गया था। जनता की वृत्ति भेद से अभेद की ओर हो चली थी। मुसलमान हिन्दुओं की राम कहानी सुनने को तैयार हो गए थे और हिन्दू मुसलमान का दास्तान हमजा।’’ सूफी काव्य की रचना के पीछे यही पूरा पसमंजर था जिसके गर्भ से इसका जन्म हुआ।
सूफी काव्य-परम्परा के पहले कवि मुल्ला दाऊद हैं। इनकी रचना का नाम ‘चंदायन’ (1379 ई.) है। चंदायन की भाषा परिष्कृत अवधी है। दूसरे प्रसिद्ध कवि मलिक मुहम्मद जायसी हैं। ‘पद्मावत’ (1540 ई.) इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है।
सूफी काव्य की विशेषताएँ:
1. सांस्कृतिक समन्वय का सूत्रपात।
2. जीवन-मूल्य के रूप में प्रेम की प्रस्तावना।
3. लोक कथाओं का प्रतीकात्मक रूपान्तरण।
4. निर्गुण ईश्वर में विश्वास।
5. गुरू (पीर) की महत्ता का प्रतिपादन।
6. प्रकृति का रागात्मक चित्रण।
7. विरह का अतिश्योक्तिपूर्ण वर्णन।
8. शैतान की अवधारणा।
9. रहस्यवादी चेतना।
10. मसनवी शैली।
इसे भी पढ़ें : शब्द शक्ति की परिभाषा और प्रकार | shabd shkti







0 टिप्पणियाँ